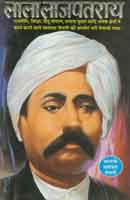|
महान व्यक्तित्व >> बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलकविनोद तिवारी
|
430 पाठक हैं |
||||||
शिक्षा को नई दिशा देने के साथ ही देश में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नारा था-स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बाल गंगाधर तिलक ने गुलामी को समग्र रूप में देखा था। देश की स्वतंत्रता
के लिए जहां तिलक ने अपनी पत्रिकाओं द्वारा मोर्चा संभाला, वहीं भारतीयों
को स्वावलंबी बनाने के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी की। भारतीयों को
एक सूत्र में बांधने के लिए ‘गणेशोत्सव’ और
‘शिवाजी
दिवस’ के रूप में किए गए उनके प्रयोग पूर्णतः सफल रहे। तिलक
द्वारा
तीनों ओर से किए गए जवाबी हमलों ने अंग्रेजी शासकों की मंशा को पूरी तरह
से झकझोर दिया। और आखिर में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा।
प्रकाशकीय
तिलक स्वतंत्रता सेनानियों के सिरमौर हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की
नीयत को संपूर्ण रूप में देखा और उसका जवाब उन्हीं की भाषा में करारे
शब्दों में दिया। ‘स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार
है’-इस
नारे का उद्घोष तिलक ने ही किया था, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया
आयाम और नई दिशा प्राप्त हुई।
आज हम स्वतंत्र हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई विदेशी हम पर शासन नहीं कर रहा है। लेकिन तिलक ने जिस आजादी की बात की थी, उस दृष्टि से हम आज भी गुलाम हैं। हमारी शिक्षा आज भी नौकरशाहों को तैयार कर रही है। नौकरी की मनोवृत्ति अधिकारों की तो बात करती है, लेकिन कर्तव्यों से मुख मोड़ लेती है। ‘सांस्कृतिक’ धरातल पर आधुनिकता का लबादा ओढ़े हम नैतिक मूल्यों को भुला रहे हैं। इसका परिणाम है-सामाजिक-सांस्कृतिक तल पर व्यक्तित्व का बिखराव। इस तरह गुलामी की स्थिति और आज जबकि हम आजाद हैं-दोनों में बाहरी बदलाव भले ही हो गया है, परंतु भीतरी तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब गुलामी का भूत सूक्ष्म रूप में हमारी नस-नस को प्रभावित कर रहा है, जिसे हम बड़े सहज रूप से बिना कोई विरोध किए हंसते-हंसते स्वीकार कर रहे हैं।
तिलक का जीवन दर्शन क्या था-इसकी संक्षिप्त परंतु सटीक जानकारी देती है यह पुस्तक। लेखक ने पुस्तक को सरस बनाने के लिए इसमें मूल घटनाओं के साथ कहीं-कहीं अपनी कल्पना का भी सहारा लिया है। उन स्थलों को इतिहास के नजरिये से न देखें, ऐसा आप पाठकों से निवेदन है।
पुस्तक से संबंधित आपके सुझावों का स्वागत है।
आज हम स्वतंत्र हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई विदेशी हम पर शासन नहीं कर रहा है। लेकिन तिलक ने जिस आजादी की बात की थी, उस दृष्टि से हम आज भी गुलाम हैं। हमारी शिक्षा आज भी नौकरशाहों को तैयार कर रही है। नौकरी की मनोवृत्ति अधिकारों की तो बात करती है, लेकिन कर्तव्यों से मुख मोड़ लेती है। ‘सांस्कृतिक’ धरातल पर आधुनिकता का लबादा ओढ़े हम नैतिक मूल्यों को भुला रहे हैं। इसका परिणाम है-सामाजिक-सांस्कृतिक तल पर व्यक्तित्व का बिखराव। इस तरह गुलामी की स्थिति और आज जबकि हम आजाद हैं-दोनों में बाहरी बदलाव भले ही हो गया है, परंतु भीतरी तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब गुलामी का भूत सूक्ष्म रूप में हमारी नस-नस को प्रभावित कर रहा है, जिसे हम बड़े सहज रूप से बिना कोई विरोध किए हंसते-हंसते स्वीकार कर रहे हैं।
तिलक का जीवन दर्शन क्या था-इसकी संक्षिप्त परंतु सटीक जानकारी देती है यह पुस्तक। लेखक ने पुस्तक को सरस बनाने के लिए इसमें मूल घटनाओं के साथ कहीं-कहीं अपनी कल्पना का भी सहारा लिया है। उन स्थलों को इतिहास के नजरिये से न देखें, ऐसा आप पाठकों से निवेदन है।
पुस्तक से संबंधित आपके सुझावों का स्वागत है।
बालगंगाधर तिलक
बालगंगाधर तिलक ने ‘गुलामी’ को उसके समग्र रूप में
देखा था।
अंग्रेजी शासक जहां एक ओर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, वहीं
दूसरी ओर तत्कालीन शिक्षा द्वारा वे नौकरों की एक नई जमात तैयार करना
चाहते थे। इतना ही नहीं, ईसाई मिशनरियों ने भारत के गरीब और पिछड़े
हिंदुओं को ईसाई बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी थी। इस प्रकार तीन तरफ से किए
जा रहे हमलों का जवाब तिलक ने सच्ची शिक्षा के रूप में दिया। उन्होंने
शिक्षा की ऐसी भूमिका तैयार की जो भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाए, उनकी
आर्थिक तंगी दूर करे, उन्हें उनके विद्रोहियों की प्रत्येक चाल की जानकारी
दे और सबसे बढ़कर उनमें भारतीय होने का गौरव जाग्रत करे।
महाराष्ट्र में ‘गणेशोत्सव’ और ‘शिवाजी उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों की प्रेरणा देकर बालगंगाधर तिलक ने भारतीयों को सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर सूत्र में बांधे रखने का शुभारंभ किया। इन उत्सवों ने उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, वह अपने आप में एक मिसाल है।
‘प्रत्येक महान पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है’-यह कहावत तिलक के संदर्भ में भी खरी उतरती है। उनकी धर्मपत्नी तापी, जिन्हें बाद में सत्यभामा नाम से पुकारा जाने लगा, ने जिन्दगी के प्रत्येक मोड़ पर तिलक का साथ दिया। तभी तो जेल में अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिलने पर कर्मठ तिलक के हृदय में छिपी प्रेम की पावन सरिता आंखों के रास्ते अजस्र रूप से बह निकली थी। इस आघात से उठी गहरी टीस ने ही उन्हें आत्मतत्व का प्रतिपादन करने वाले पवित्र ग्रंथ ‘श्रीमद्भागवद्गीता’ के रहस्यों का खुलासा करने को प्रेरित किया। इस घटना के बाद उन्होंने स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण रूप से झोंक दिया।
गंगाधर को सच कहने से कोई नहीं रोक सकता था-न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई परिस्थिति। सच्चाई का सख्ती से पालन करने और करवाने के कारण ही बालगंगाधर के मित्र उन्हें मिस्टर ब्लंट कहा करते थे। सच बोलने से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों से वे कभी घबराए नहीं, बल्कि उनका प्रयोग उन्होंने अपने ज्ञान तराशने के लिए किया। भारतीय संस्कृति की महानतम विरासत ‘श्रीमद्भगवद्गीता पर लिखी गई टीका ‘गीता रहस्य’ उनकी प्रतिभा ज्ञान और कर्म के प्रति निष्ठा का अनमोल उदाहरण है।
महाराष्ट्र में ‘गणेशोत्सव’ और ‘शिवाजी उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों की प्रेरणा देकर बालगंगाधर तिलक ने भारतीयों को सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर सूत्र में बांधे रखने का शुभारंभ किया। इन उत्सवों ने उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, वह अपने आप में एक मिसाल है।
‘प्रत्येक महान पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है’-यह कहावत तिलक के संदर्भ में भी खरी उतरती है। उनकी धर्मपत्नी तापी, जिन्हें बाद में सत्यभामा नाम से पुकारा जाने लगा, ने जिन्दगी के प्रत्येक मोड़ पर तिलक का साथ दिया। तभी तो जेल में अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिलने पर कर्मठ तिलक के हृदय में छिपी प्रेम की पावन सरिता आंखों के रास्ते अजस्र रूप से बह निकली थी। इस आघात से उठी गहरी टीस ने ही उन्हें आत्मतत्व का प्रतिपादन करने वाले पवित्र ग्रंथ ‘श्रीमद्भागवद्गीता’ के रहस्यों का खुलासा करने को प्रेरित किया। इस घटना के बाद उन्होंने स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण रूप से झोंक दिया।
गंगाधर को सच कहने से कोई नहीं रोक सकता था-न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई परिस्थिति। सच्चाई का सख्ती से पालन करने और करवाने के कारण ही बालगंगाधर के मित्र उन्हें मिस्टर ब्लंट कहा करते थे। सच बोलने से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों से वे कभी घबराए नहीं, बल्कि उनका प्रयोग उन्होंने अपने ज्ञान तराशने के लिए किया। भारतीय संस्कृति की महानतम विरासत ‘श्रीमद्भगवद्गीता पर लिखी गई टीका ‘गीता रहस्य’ उनकी प्रतिभा ज्ञान और कर्म के प्रति निष्ठा का अनमोल उदाहरण है।
बाल गंगाधर तिलक
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गंगाधर पंत का परिवार रहता था।
रत्नागिरी की एक मराठी पाठशाला में गंगाधर पंत प्रधानाचार्य की हैसियत से
कार्यरत थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी। गंगाधर पंत ने कभी सपने में भी नहीं
सोचा था कि जन्म लेने वाला यह बालक एक दिन स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा
साबित होगा और ‘स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार
है’ का
नारा पूरे देश में बुलंद करेगा।
जन्म और शिक्षा
समय ने करवट बदली। 23 जुलाई, सन् 1856 को गंगाधर की पत्नी ने एक पुत्र को
जन्म दिया। बालक की किलकारी से घर में एक नई रोशनी जगमग हो गई थी। इस
रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भारत में तेजी से बढ़ रहे अंग्रेजों के
अत्याचार अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे।
बालक का लालन-पालन होता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। इसी बीच बालक स्कूल जाने लायक हो गया। गंगाधर पंत ने बालक का दाखिला रत्नागिरी की एक पाठशाला में करवा दिया। वे बालक को प्यार से बाल गंगाधर कहकर बुलाते थे। गंगाधर के पिता उसे रोज भारत के गुलाम होने की बातें बताते थे। यह सुनकर गंगाधर गंभीर हो जाता था। जब वह स्कूल जाता तो वहीं बातें स्कूल के बच्चों की भी बताता। उन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि उनका प्यारा भारत गुलाम है। इसलिए वे गंगाधर की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे।
एक दिन गंगाधर स्कूल से घर, तो उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने उसे आशीर्वाद देकर कहा-
‘‘बेटा ! रत्नागिरी से मेरा तबादला पुणे कर दिया गया है। इसलिए तुम अब पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई करोगे।’’
‘‘पिताजी ! मेरे यहाँ के सभी साथी यहाँ छूट जाएंगे। मुझे इनकी बड़ी याद आएगी। इनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा।’’ गंगाधर ने अपने पिता से कहा।
‘‘पुत्र ! जो जहाँ रहता है, वह वहीं अपने साथी बना लेता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पुणे के जिस विद्यालय में पढ़ोगे, वहाँ तुम्हारे कई साथी बन जाएंगे। फिर शायद तुम इन्हें भूल जाओ।’’ पिता ने अपने पुत्र को समझाया।
पिता की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वह अपने इन साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ना चाहता था। यह बात उसके दिलो-दिमाग में घर कर गई थी। इस बात को बिना किसी को बताए वह अपने मन में विचार-विमर्श करने लगा। वह चुपचाप अपने पिताजी के साथ पुणे चला आया, किंतु यहां आकर उसे उदासी ने घेर लिया।
गंगाधर को अपने पुराने साथियों की बड़ी याद आती थी। ऐसे में वह मन मारकर रह जाता था, किंतु कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे उसकी उदासी दूर होने लगी। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके नए दोस्त बन गए। वह अपने नए-नए दोस्तों के साथ भावी जीवन के सपने बुनने लगा।
उसी समय गंगाधर पर ईश्वर ने एक ऐसा वज्राघात किया, जिससे उसका दिल दहल गया। जिस माँ ने उसे पाल-पोसकर इतना बड़ा किया था, जो मां उसे लोरियां गा-गाकर सुलाती थी, आज वहीं मां इस मायारूपी दुनिया से चल बसी। गंगाधर को इससे बड़ा आघात पहुंचा।
बाद में गंगाधर की चाची ने उसे माँ का प्यार दिया। जैसे-जैसे उसे चाची का प्यार मिलता रहा, वैसे-वैसे वह अपनी माँ की यादों को भूलता रहा। अब वह पुणे के अपने नए दोस्तों से देश के हालात पर चर्चा करता। उसके स्कूल के अध्यापक भी कभी-कभी देश के हालातों पर टीका-टिप्पणी कर दिया करते थे। उनका कहना था कि अंग्रेजों के अत्याचार कितने भी बढ़ जाएं, उन्हें एक न एक दिन भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
जो देशद्रोही थे। वे भारत के कभी आजाद न होने की बात करते थे। वे देश की कमजोरियां अंग्रेजों के सामने उजागर करते थे। इससे अंग्रेजों का हौसला और बढ़ जाता था।
देशद्रोही लोग क्रांति की बात करने वाले नौजवानों से बहुत चिढ़ते थे। उस समय गंगाधर 15 वर्ष का हो गया था। उन दिनों बाल-विवाह करने की परंपरा थी। अतः गंगाधर के पिता ने भी पुत्र के विवाह को लेकर जल्दबाजी दिखाई। इतनी छोटी आयु में गंगाधर को यह भी नहीं मालूम था कि विवाह का अर्थ क्या है ? लेकिन पिता की बीमारी की हालत को देखकर उसने उनके फैसले पर सहमति दे दी।
बालक का लालन-पालन होता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। इसी बीच बालक स्कूल जाने लायक हो गया। गंगाधर पंत ने बालक का दाखिला रत्नागिरी की एक पाठशाला में करवा दिया। वे बालक को प्यार से बाल गंगाधर कहकर बुलाते थे। गंगाधर के पिता उसे रोज भारत के गुलाम होने की बातें बताते थे। यह सुनकर गंगाधर गंभीर हो जाता था। जब वह स्कूल जाता तो वहीं बातें स्कूल के बच्चों की भी बताता। उन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि उनका प्यारा भारत गुलाम है। इसलिए वे गंगाधर की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे।
एक दिन गंगाधर स्कूल से घर, तो उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने उसे आशीर्वाद देकर कहा-
‘‘बेटा ! रत्नागिरी से मेरा तबादला पुणे कर दिया गया है। इसलिए तुम अब पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई करोगे।’’
‘‘पिताजी ! मेरे यहाँ के सभी साथी यहाँ छूट जाएंगे। मुझे इनकी बड़ी याद आएगी। इनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा।’’ गंगाधर ने अपने पिता से कहा।
‘‘पुत्र ! जो जहाँ रहता है, वह वहीं अपने साथी बना लेता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पुणे के जिस विद्यालय में पढ़ोगे, वहाँ तुम्हारे कई साथी बन जाएंगे। फिर शायद तुम इन्हें भूल जाओ।’’ पिता ने अपने पुत्र को समझाया।
पिता की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वह अपने इन साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ना चाहता था। यह बात उसके दिलो-दिमाग में घर कर गई थी। इस बात को बिना किसी को बताए वह अपने मन में विचार-विमर्श करने लगा। वह चुपचाप अपने पिताजी के साथ पुणे चला आया, किंतु यहां आकर उसे उदासी ने घेर लिया।
गंगाधर को अपने पुराने साथियों की बड़ी याद आती थी। ऐसे में वह मन मारकर रह जाता था, किंतु कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे उसकी उदासी दूर होने लगी। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके नए दोस्त बन गए। वह अपने नए-नए दोस्तों के साथ भावी जीवन के सपने बुनने लगा।
उसी समय गंगाधर पर ईश्वर ने एक ऐसा वज्राघात किया, जिससे उसका दिल दहल गया। जिस माँ ने उसे पाल-पोसकर इतना बड़ा किया था, जो मां उसे लोरियां गा-गाकर सुलाती थी, आज वहीं मां इस मायारूपी दुनिया से चल बसी। गंगाधर को इससे बड़ा आघात पहुंचा।
बाद में गंगाधर की चाची ने उसे माँ का प्यार दिया। जैसे-जैसे उसे चाची का प्यार मिलता रहा, वैसे-वैसे वह अपनी माँ की यादों को भूलता रहा। अब वह पुणे के अपने नए दोस्तों से देश के हालात पर चर्चा करता। उसके स्कूल के अध्यापक भी कभी-कभी देश के हालातों पर टीका-टिप्पणी कर दिया करते थे। उनका कहना था कि अंग्रेजों के अत्याचार कितने भी बढ़ जाएं, उन्हें एक न एक दिन भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
जो देशद्रोही थे। वे भारत के कभी आजाद न होने की बात करते थे। वे देश की कमजोरियां अंग्रेजों के सामने उजागर करते थे। इससे अंग्रेजों का हौसला और बढ़ जाता था।
देशद्रोही लोग क्रांति की बात करने वाले नौजवानों से बहुत चिढ़ते थे। उस समय गंगाधर 15 वर्ष का हो गया था। उन दिनों बाल-विवाह करने की परंपरा थी। अतः गंगाधर के पिता ने भी पुत्र के विवाह को लेकर जल्दबाजी दिखाई। इतनी छोटी आयु में गंगाधर को यह भी नहीं मालूम था कि विवाह का अर्थ क्या है ? लेकिन पिता की बीमारी की हालत को देखकर उसने उनके फैसले पर सहमति दे दी।
विवाह
गंगाधर का विवाह गांव की एक भोली-भाली तापी नामक कन्या से हुआ था। तापी की
उम्र मात्र दस वर्ष की थी। अभी वह बचपन की दहलीज को पार नहीं कर पाई थी कि
तभी उस बालिका को वधू बना दिया गया। विदाई के समय वह इतना भी नहीं समझ पाई
कि उसे सजाया-संवारा क्यों जा रहा है ? उसका विवाह हिन्दू समाज के
रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ था, क्योंकि दोनों परिवार ब्राह्मण जाति से
ताल्लुक रखते थे। जब वह डोली में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक
दिखाई पड़ी। न जाने क्या सोचकर वह खिल-खिलाकर हंसने लगी। किंतु जब उसने
अपने माता-पिता को आंसू बहाते देखा तो उसके कोमल हृदय को भी ठेस लगी और
उसकी आँखों में भी आंसू आ गए।
तापी नादान होने के कारण यह नहीं समझ पाई कि उसके मां-बाप क्यों रो रहे हैं ? उसे इतना अनुमान अवश्य था कि गंगाधर के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध गई है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह सुन्दर कपड़ों में सजी-धजी एक खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। उसके पिता उसके मेहंदी लगे हाथों को चूमकर वहां से हट चुके थे। उसकी माँ और दादी का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। तभी कहार उसकी डोली उठाकर वहां से आगे बढ़ गए।
तापी के साथ एक अधेड़ उम्र की स्त्री भी उसकी डोली में आई थी। जब बाल गंगाधर तापी के पास गए तो उनसे कुछ कहना चाहा पर वह मारे शर्म के कुछ न बोल सकी। गंगाधर को अब यह मालूम हो गया था कि उनका विवाह हुआ है। उन्हें तापी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उसके चेहरे को देखकर उन्हें ऐसा लगता, जैसे आसमान में पूर्णमासी का चांद खिल गया हो। उन्हें कभी अपने स्कूल के लड़के-लड़कियों से बात करने में शर्म नहीं आई। पर आज वे तापी से बात करने में शर्म महसूस कर रहे थे।
तापी जब अपनी माँ की याद में रोने लगती, तो गंगाधर का कलेजा कांप उठता था। लेकिन उनके दिल में यह प्रश्न उठने लगता था कि तापी को मेरे पिताजी उसके घर से यहां क्यों लाए हैं ? परंतु वे उसे अपने से दूर करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें तापी से आत्मिक लगाव हो गया था। तीन दिन वह उनके घर रही। उसके बाद वह अपनी माँ के घर चली गई।
तापी, गंगाधर से यह वादा कर चुकी थी कि अब वह पढ़-लिखकर उनके घर आएगी। उसके जाने के बाद गंगाधर मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगे। तापी ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात कही। उसके मां ने बेटी की भावनाओं की कद्र करते हुए उसे शिक्षा दिलाना आरंभ कर दिया।
तापी माँ के साथ रहने-रहते सब कुछ भूल गई। यहां तक कि उसे अपनी शादी की बात भी याद नहीं रही। पर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हमेशा उठता रहता था। लेकिन कभी वह इसका अर्थ नहीं समझ पाई। जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी तो कभी-कभी कोई सहेली उसकी शादी की बात छेड़ देती थी, फिर उसे अपने विवाह का स्मरण हो आता था।
समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। तापी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। उधर, गंगाधर की अंतःचेतना उन्हें ऐसी दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्हें देश की सामाजिक स्थिति का पता चल चुका था। शिक्षा का अभाव, गरीबी, कुप्रथाओं का बोलबाला आदि जैसी कई समस्याएं समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ी थीं, जबकि अंग्रेजी हुकूमत राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं से गंगाधर अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे। अतः वे उनसे निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गए।
तापी नादान होने के कारण यह नहीं समझ पाई कि उसके मां-बाप क्यों रो रहे हैं ? उसे इतना अनुमान अवश्य था कि गंगाधर के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध गई है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह सुन्दर कपड़ों में सजी-धजी एक खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। उसके पिता उसके मेहंदी लगे हाथों को चूमकर वहां से हट चुके थे। उसकी माँ और दादी का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। तभी कहार उसकी डोली उठाकर वहां से आगे बढ़ गए।
तापी के साथ एक अधेड़ उम्र की स्त्री भी उसकी डोली में आई थी। जब बाल गंगाधर तापी के पास गए तो उनसे कुछ कहना चाहा पर वह मारे शर्म के कुछ न बोल सकी। गंगाधर को अब यह मालूम हो गया था कि उनका विवाह हुआ है। उन्हें तापी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उसके चेहरे को देखकर उन्हें ऐसा लगता, जैसे आसमान में पूर्णमासी का चांद खिल गया हो। उन्हें कभी अपने स्कूल के लड़के-लड़कियों से बात करने में शर्म नहीं आई। पर आज वे तापी से बात करने में शर्म महसूस कर रहे थे।
तापी जब अपनी माँ की याद में रोने लगती, तो गंगाधर का कलेजा कांप उठता था। लेकिन उनके दिल में यह प्रश्न उठने लगता था कि तापी को मेरे पिताजी उसके घर से यहां क्यों लाए हैं ? परंतु वे उसे अपने से दूर करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें तापी से आत्मिक लगाव हो गया था। तीन दिन वह उनके घर रही। उसके बाद वह अपनी माँ के घर चली गई।
तापी, गंगाधर से यह वादा कर चुकी थी कि अब वह पढ़-लिखकर उनके घर आएगी। उसके जाने के बाद गंगाधर मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगे। तापी ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात कही। उसके मां ने बेटी की भावनाओं की कद्र करते हुए उसे शिक्षा दिलाना आरंभ कर दिया।
तापी माँ के साथ रहने-रहते सब कुछ भूल गई। यहां तक कि उसे अपनी शादी की बात भी याद नहीं रही। पर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हमेशा उठता रहता था। लेकिन कभी वह इसका अर्थ नहीं समझ पाई। जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी तो कभी-कभी कोई सहेली उसकी शादी की बात छेड़ देती थी, फिर उसे अपने विवाह का स्मरण हो आता था।
समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। तापी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। उधर, गंगाधर की अंतःचेतना उन्हें ऐसी दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्हें देश की सामाजिक स्थिति का पता चल चुका था। शिक्षा का अभाव, गरीबी, कुप्रथाओं का बोलबाला आदि जैसी कई समस्याएं समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ी थीं, जबकि अंग्रेजी हुकूमत राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं से गंगाधर अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे। अतः वे उनसे निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गए।
आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार
गंगाधर में गजब का आत्मविश्वास था। उनकी बातें सुनकर उनके पिता बड़े
आश्वस्त होते थे। गंगाधर के नेक विचार, आदतें, और अदम्य साहस को देखकर
उन्हें यही लगता था कि एक दिन उनका बेटा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि
प्राप्त करेगा और अपने कुल तथा देश का नाम रोशन करेगा।
जब से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया था, तब से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। होनी टल न सकी। मूक बना कालचक्र सब कुछ देखता रहा, बड़ी-बड़ी दवाएं फेल हो गईं। ऐसे में गंगाधर के पिता ईश्वर को प्यारे हो गए।
पिता की मृत्यु से गंगाधर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस असीम दुख ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उनके भाई-बहन बड़ी मुश्किल से इस दुख को बरदाश्त कर पाए। गंगाधर की चाची-रोते-रोते बेहोश हो गईं। दुखद सूचना पाकर तापी के पिता उसे लेकर गंगाधर के घर पहुंचे। गंगाधर की चाची के कहने पर वे तापी को छोड़कर वापस चले गए।
जब से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया था, तब से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। होनी टल न सकी। मूक बना कालचक्र सब कुछ देखता रहा, बड़ी-बड़ी दवाएं फेल हो गईं। ऐसे में गंगाधर के पिता ईश्वर को प्यारे हो गए।
पिता की मृत्यु से गंगाधर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस असीम दुख ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उनके भाई-बहन बड़ी मुश्किल से इस दुख को बरदाश्त कर पाए। गंगाधर की चाची-रोते-रोते बेहोश हो गईं। दुखद सूचना पाकर तापी के पिता उसे लेकर गंगाधर के घर पहुंचे। गंगाधर की चाची के कहने पर वे तापी को छोड़कर वापस चले गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book